पाकिस्तान के मूल में ही द्वेष
 निशिकांत ठाकुर
निशिकांत ठाकुर
भारत विभाजन के लगभग तय हो जाने पर न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता हरबर्ट एल मैथ्यूज जिन्ना से मिले। बातचीत के क्रम में उन्होंने जिन्ना का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट किया जिन पर तमाम लोगों का भविष्य निर्भर करता था। उन सबका जिन्हें उन प्रदेशों में रहना था जो पूरे भारत से अलग किए जाते। मैथ्यूज ने इस पर स्पष्ट सवाल किया। तब जिन्ना ने कहा, “अफगानिस्तान गरीब देश है तो भी उसका निर्वाह हो ही जाता है। इराक की भी वही हालत है। यद्यपि इसकी आबादी हमारी सात करोड़ की आबादी का एक छोटा हिस्सा ही है। यदि हम लोग आजाद होकर गरीब ही रहना चाहते हैं तो इसमें हिंदुओं को क्या आपत्ति है? अर्थव्यवस्था अपनी देखभाल स्वयं कर लेगी।”
बहस के लिए इस प्रकार के उदगार भले ही प्रकट किए जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रश्न पर सात करोड़ मुसलमानों का सारा भविष्य निर्भर करता हो, उसे इतने अगंभीर ढंग से टाल देना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। जिन्ना बैरिस्टर थे, लेकिन जब वह इस बात के लिए अडिग थे कि एक राष्ट्र मुसलमानों का हो जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। उनकी इस जिद ने देश का विभाजन अनिवार्य कर दिया। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भारत पर उसका राज कायम रहे और आजादी ही न मिले। मिले तो कई खंडों में, और नहीं तो कम से कम दो खंडों में तो देश का बँटवारा हो ही जाए। इसीलिए चर्चिल हर जगह यह डींग हाँकता फिरता था कि भारत को चलाने के लिए वहाँ के लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। आजादी के बाद यह देश खंड-खंड में बँटकर स्वतः नष्ट हो जाएगा।
कुछ लोगों का कहना है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए इकबाल ने पहले पहल स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग पेश की थी। उन्होंने कहा मुसलमानों का धार्मिक आदर्श उसी सामाजिक संगठन पर निर्भर करता है जिसका उसके ही द्वारा निर्माण हुआ है। आप एक को यदि ठुकरा देते हैं तो दूसरे को भी ठुकरा देना होगा। इसलिए जिस राष्ट्रीयता में मुसलमानों को इस्लाम के सिद्धांतों की हत्या करनी पड़े, उस पर तो उन्हे विचार ही नहीं करना चाहिए। भारतीय राष्ट्र की एकता का आधार बहुतों के साथ मेल और संगठन होना चाहिए, न कि उसका विरोध। इसी तरह की एकता पर भारत और उसके साथ ही समस्त एशिया का भविष्य निर्भर करता है। सच यह है कि इकबाल का अपनी बात ही अंतर्विरोधों से भरी हुई थी और यह केवल यहीं तक सीमित नहीं था। वस्तुस्थिति यह है कि भारत के प्रति वस्तुगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण जाहिर करना सांप्रदायिक इकबाल के क्षुद्र स्वार्थों के अनुरूप नहीं था।
इसलिए वे पूरी तरह एकांगी और हवाई यूरोपीय नजरिये का समर्थन करते हुए कहते थे कि हमें यह कहते हुए खेद होता है कि इस दिशा में हमारा अब तक का प्रयास हर तरह से असफल रहा। वे असफल क्यों हुए – कदाचित हम लोग एक दूसरे पर संदेह करते हैं और उस पर हावी होकर रहना चाहते हैं। परस्पर सहयोग के ऊँचे आदर्श के लिए भी शायद हम लोग उन विशेषाधिकारों का त्याग नही करना चाहते जो भाग्य से हमारे साथ आ गए हैं और अपनी स्वार्थपरता को राष्ट्रीयता का आवरण से ढककर रखना चाहते हैं। बाहर से तो हम लोग उदार राष्ट्रीयता की डींग हांकते हैं, लेकिन अंदर से कट्टर सांप्रदायिक हैं। यूरोपीय देशों के अनुसार भारतीय समाज की इकाई भौमिक नहीं है। इसलिए सांप्रदायिक गुटों को मान्यता दी। यूरोपीय जनशासन का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो सकता। इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों को मुस्लिम भारत की माँग सर्वथा उचित है।
यह बीज कुछ उन मुसलमान युवकों के दिमाग में बैठ गया जो संघ-राष्ट्र के विरोधी थे और जिनकी यह धारणा थी कि शासन-विधान में जो संरक्षण दिए जा रहे हैं, वे व्यर्थ हैं और बहादुर तथा मूक मुसलमान जाति हिंदू राष्ट्रीयता की वेदी पर बलिदान की जा रही है। पंजाबी मुसलमान चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों को एक स्वतंत्र राष्ट्र कहना शुरू कर दिया जो अब तक अल्पसंख्यक समुदाय माने जाते थे। इकबाल के विचार से यह एकदम भिन्न था। उनका प्रस्ताव था कि इन प्रांतों को मिलाकर एक राज्य कायम किया जाए जो अखिल भारतीय राष्ट्र संघ का एक अंग हो और चौधरी रहमत अली का प्रस्ताव था कि इन प्रांतों का अपना अलग संघ शासन ही हो।
वर्ष 1933 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के समक्ष बयान देते हुए मुस्लिम गवाहों ने पाकिस्तान योजना के बारे में निम्नलिखित मत प्रकट किया था–ए युसूफ अली — जहाँ तक मेरी धारणा है, यह कच्चे मस्तिष्क वाले विद्यार्थियों की योजना है। इसे किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने पेश नहीं किया है। डॉक्टर खलीफा शुजाउद्दीन – शायद इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि उस तरह की किसी भी योजना पर किसी भी संस्था या प्रतिनिधि जमात ने विचार नहीं किया है। विभाजन की भावना का उदय और विकास चाहे किसी भी प्रकार हुआ हो, लेकिन डॉ. अंसारी के शब्दों में निःसंदेह कहा जा सकता है कि इस बीज को उपजाऊ भूमि मिल गई और इसने अपनी ओर जबरदस्ती ध्यान आकृष्ट कर लिया।
फिर बात नहीं बनी और भारत का दो खंडों में बँटना तय हों गया। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे।
इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था फिर 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए जो कि अभिजित मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11 बजकर 51 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 15 मिनट तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12 बजकर 39 मिनट तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था।
शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। खासकर, तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर्वस्थगित कर दें। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से अवाम आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था।
आजादी के बाद भारत अब तक चार बार अपने दुश्मनों से सीधे युद्ध स्थल पर टक्कर ले चुका है। हर बार पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी है। आइए, जानते हैं कि 1947 से 1999 तक क्या है भारत के युद्धों का इतिहास? भारत पर पहला युद्ध आजादी के एक साल बाद ही थोप दिया गया था। जब पाकिस्तान से आए कबीलाई लड़ाकों के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध 441 दिनों तक चला, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध भारत ने साल 1971 में लड़ा था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के तौर पर अस्तित्व में आया था। ये युद्ध महज 13 दिनों तक चला और पाकिस्तान की सेना के 93000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। चौथा और आखिरी युद्ध भी भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल की चोटियों पर लड़ा। मुशर्रफ की शह पर आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की और कब्जा जमा लिया। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय सेना और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये युद्ध 85 दिनों तक चला और पाकिस्तान को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी।
(इस लेख में कुछ ऐतिहासिक तथ्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक “खंडित भारत” से साभार लिए गए हैं)।
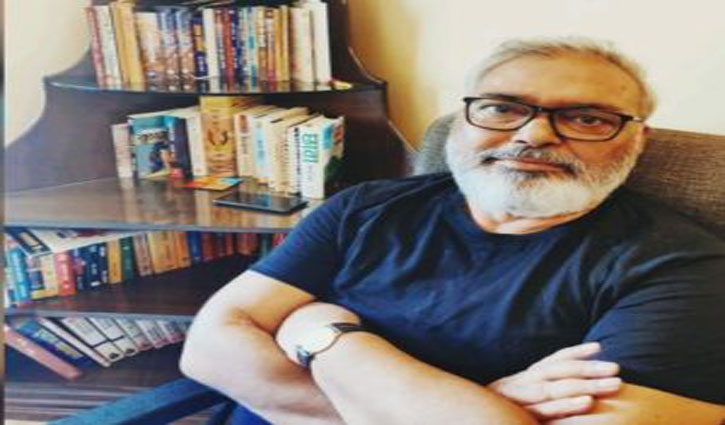 (लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)।



